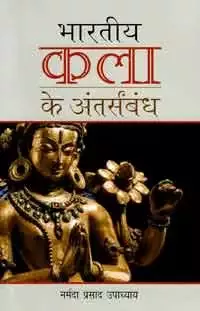|
जीवनी/आत्मकथा >> रस-पुरुष पं. विद्यानिवास मिश्र रस-पुरुष पं. विद्यानिवास मिश्रनर्मदा प्रसाद उपाध्याय
|
341 पाठक हैं |
||||||
पं. विद्यानिवास मिश्र के अनन्य स्नेहभाजन और आलोक-पुत्र श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय द्वारा उनके जीवन के रस और भाव का दिग्दर्शन कराती भावपूर्ण पुस्तक।
महाप्रयाण का अर्थ उनके संदर्भ में मुझे यही लगता है कि कहीं उन्हें
पाणिनि न मिल गए हों, जिनकी व्याकरण तकनीक की गलियों में अपने यौवन में वे
उलझ गए थे। कहीं भवभूति न मिल गए हों, जिनके राम के मुकुट को बारिश में
भीगते हुए देखकर वे कभी कठोर नहीं हो पाए। कहीं कालिदास न मिल गए हों,
जिनसे साक्षात्कार करते हुए वे शकुंतला के उस श्रमसिंचित सौंदर्य को
निहारने लगे हों, जिस पर कभी दुष्यंत इसलिए रीझ गए थे कि वह तपस्वी बाला
अपने उपवन के वृक्षों को पानी देते ठिठककर एक हाथ में ढीले केशों में
खोंसे हुए शिरीष के फूल को संभाल रही थी और दूसरे से अपने मस्तक पर आई
पसीने की बूँदों को पोंछने का यत्न कर रही थी। कहीं राहुल न मिल गए हों,
जिनसे शब्दकोश की चर्चा चल पड़ी हो, कहीं नागार्जुन से मुलाकात न हो गई
हो, जिनसे भोजपुरी में वे बतियाने बैठ गए हों। कहीं अज्ञेय न टकरा गए हों,
जिनके सामने वे लौटने की जिद्द नहीं कर सकते, और कहीं अनिकेत नवीन न मिल
गए हों, जिन्होंने कहा हो कि तुम भी अनिकेतन हो, क्या करोगे लौटकर ?
—इसी संग्रह से
पं. विद्यानिवास मिश्र के अनन्य स्नेहभाजन और आलोक-पुत्र श्री नर्मदा
प्रसाद उपाध्याय द्वारा उनके जीवन के रस और भाव का दिग्दर्शन कराती
भावपूर्ण पुस्तक।
पं. पिद्यानिवास मिश्र
यात्राओं के महायात्री
विरासत, परंपरा और जातीय-बोध पहचान होते हैं किसी देश और उसके निवासियों
की अस्मिता के। ये उस देश और व्यक्ति के विकास के सच्चे अर्थों में
आख्याता होते हैं। विद्रोह न तो विरासत से, न सच्ची परंपरा से और न
जातीयता से हो सकता है। वह हो सकता है तो जड़ता से, रूढ़ि से और
अवैज्ञानिकता से। समुद्र और आकाश धरती की विरासत हैं, तरंगों का उठना और
आकाश-गंगा का चमकना इस विरासत की परंपराएँ हैं और इस धरती की
प्राण-प्रतिष्ठा करनेवाले जंगल और उनमें गूँजता पक्षियों का कलरव वह जातीय
बोध है,जो धरती को प्राणवान् कहलाने का गौरव देता है और इस दृष्टि का
आख्यान करनेवाले बिरले द्रष्टा पं. विद्यानिवास मिश्र जैसे वे मनीषी होते
हैं तो अपने आप में एक समग्र सांस्कृतिक युग बन जाते हैं। उनका जाना एक
पहचान करानेवाले का सदैव के लिए चले जाना है। बिना किसी मुखौटे के अपनी
पहचान से रू-ब-रू कराने के लिए आजीवन जूझनेवाला एक यायावर जुझारू
व्यक्तित्व हमारे बीच से यात्रा करते-करते महायात्रा पर चला गया।
सौ से ज्यादा उनकी पुस्तकें हैं। ये धर्म, भाषा, संस्कृति, कला और लोक से लेकर हमारे व्यवहार तक पर लिखी गई हैं। वे इस देश की मनीषा के प्रतिमान व्यक्तित्व थे। ‘पद्मभूषण’ से लेकर साहित्य अकादेमी की महत्तर सदस्यता से सम्मानित उनका वैदुष्य किसी व्याख्या का मोहताज नहीं है। उनकी मनीषा इतनी प्रखर थी कि उसकी परिधि में पूरा विश्व आया। वे पूरा विश्व घूमे और हर देश में उन्होंने अपनी दृष्टि से इस देश की पहचान को स्थापित करने का ईमानदार यत्न किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद हिंदी में यही एक ऐसा व्यक्तित्व हुआ, जिसकी बहुआयामी प्रतिभा ने हमारे तमाम अनुसासनों को जोड़ने की कोशिश की। खंड से विद्रोह और समग्र के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण अपने कृतित्व के माध्यम से जताया।
हिंदी में निबंध, और विशेष रूप से ललित-निबंध, की परंपरा को उन्होंने नए धरातल पर स्थापित किया। उनकी मान्यता स्पष्ट थी। वे अडिग, आस्थावादी थे। वे कहते थे कि ‘‘वैदिक सूक्तों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविछिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है, उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। मेरी मान्यताओं का वही शाश्वत आधार है। मैं रेती में अपनी डोंगी नहीं चलाना चाहता और न जमीन के ऊपर बने रुँधे तालाबों में छपकोरी खेलना चाहता हूँ। इसलिए प्रचलित शब्दावली में अगर प्रगतिशील नहीं हूँ तो कम-से-कम प्रतिगामी भी नहीं हूँ।’’ उनके साथ रहते, उनको पढ़ते, उनसे बातें करते मैंने अनुभव किया कि उनके आचरण को कहीं उनकी अभिव्यक्ति से जोड़कर देखा गया और इसके कारण उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में नहीं समझा जा सका। वे कोरे पंक्तिपावन ब्राह्मण नहीं थे। अपने संस्कारों से वे गहरे जुड़े थे। लेकिन उनमें वैचारिक संकीर्णता नहीं थी। उनकी ग्रहणशीलता अद्भुत थी, उनका औदार्य विलक्षण था और उनकी अछोर करुणा आकाश की तरह असीम थी। वे आई.सी.एस. में जा सकते थे, लेकिन वे राहुलजी के साथ हो लिये। यायावरी करा पाठ उन्हीं से सीखा। डॉ. राममनोहर लोहिया से उनका निकट संपर्क था और रफी अहमद किदवई उनके आदर्श राजनीतिज्ञ थे। नवीनजी उनके सबसे अनन्य मित्र थे। बात-बात में नवीनजी का उद्धरण देते। ‘साहित्य अमृत’ का एक पूरा अंक ही उन्होंने नवीनजी पर निकाला। धूमिल के एक काव्य-संग्रह की उन्होंने भूमिका भी लिखा, यह जानकारी भी मुझे उनके मित्रों ने दी। स्व. श्रीपतराय उनके अभिन्न मित्र थे। यह तथ्य उनके अनुज श्री महेश्वर मिश्र ने उनके निधन के बाद मुझे बताया कि प्रेमचंद की कृतियों का सर्वप्रथम संकलन व संपादन उन्होंने पूरे मनोयोग से श्रीपतरायजी के लिए क्या और कहीं भी अपना नाम न आने का वचन श्रीपतरायजी से लिया। इस कार्य के लिए वे जो कुछ कर सकते थे, करते रहे। आशय यही है कि इन तथ्यों के आधार पर इतना जरूर जाना जा सकता है कि वे कट्टरपंथी और जड़ सर्जक नहीं थे। उनकी मान्यताएँ, उनके विश्वास और उनकी आस्था अपनी जगह स्पष्ट थी। कहीं कोई कुहासा नहीं था, भ्रम नहीं था, समझौते नहीं थे। वे अपनी जमीन पर देवदारु के वृक्ष की तरह आजीवन तने खड़े रहे।
ललित-निबंध उनकी प्रिय विद्या थी। ललित-निबंध को वे व्यक्ति-व्यंजक निबंध का छोटा सा प्रकार मानते थे। वे कहते थे कि कभी-कभी सुंदर से असुंदर अधिक छूता है। उसी तरह ललित से अधिक मनुष्य के हाथ से अनसँवरा छूता है, अनतराशा हीरा तराशे हीरे से अधिक मूल्यवान् लगता है। व्यक्ति की दृष्टि में सुंदर या ललित हो जाए—यही उनका उद्देश्य रहा। उनके लिए लिखना मरना या मरने जैसी यातना की तरह था। वे कहते थे, ‘‘अपने अनुभवों को उघारना मौत से बड़ी यंत्रणा है।’’ उन्होंने ‘स्तवक’ शीर्षक से व्यक्ति-व्यंजक निबंधों का संकलन डॉ. परमानंद श्रीवास्तव के सहयोग से निकाला, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर कुबेरनाथ राय तक के निबंध-लेखकों के प्रतिनिधि निबंध संकलित किए। हाल ही में उनके निबंधों का एक संकलन ‘व्यक्ति-व्यंजना’ के नाम से प्रकाशित हुआ है, जिसमें उनके चुने हुए 53 निबंध संकलित हैं। तब मैंने उनसे इस ग्रंथ के प्रकाशन के समय एक लंबी बात की थी। उनसे पूछा था कि आगामी सदी के भारत को वे किस रूप में देखना चाहते हैं ? उन्होंने कहा था कि मैं तो आज के अत्यंत संधिःकालीन भारत में संभावनाओं की तलाश करना चाहता हूँ। बेकार के आरोपित कालखंडों में कैद सूर्योदय की बात नहीं सोचता। उनके निबंध द्विवेदीजी की परंपरा को बहुत आगे ले जाते हैं। कुबेरनाथ राय और विवेकी राय जैसे समकालीन निबंध-लेखकों के साथ उनकी त्रयी बनती है। ठीक उसी तरह जिस तरह हरिशंकर परसाई, रवींद्रनाथ त्यागी और शरद जोशी की त्रयी व्यंग्य लेखन में है। यों निबंध विधा हमारे समकालीन लेखन में प्रायः उपेक्षित है; लेकिन यदि इस विधा की धारा नहीं सूख पाई, बल्कि और प्रवाहमय होती रही तो निस्संदेह इसका श्रेय उन्हें दिया जाना चाहिए। ‘नवभारत टाइम्स’ और ‘साहित्य अमृत’ के प्रधान संपादक के बतौर उन्होंने निबंधों को प्रमुखता से छापा। आज के जो थोड़े-बहुत निबंधकार हैं, उन्हें उन्होंने प्रश्रय दिया, उनकी हौसला-आफजाई की। अंग्रेजी के ‘पर्सनल ऐसे’ की विशेतओं से परिचित कराते हुए उन्होंने हिंदी के व्यक्ति-व्यंजक निबंधों की मौलिक परंपराओं को उद्घाटित किया और यह सिद्ध करने की कोशिश की कि हिंदी की प्रकृति के स्वतंत्र विकास का प्रमाण हिंदी में रचे गए मौलिक निबंध हैं।
उनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं—‘छितवन की छाँह’, ‘अंगद की नियति’, ‘आँगन का पंछी और बंजारा मन’, ‘कँटीले तारों के आर-पार’, ‘कौन तू फुलवा बीननिहारी’, ‘गाँव का मन’, ‘मेरे राम का मुकुट भीग रहा है’, ‘तमाल के झरोखे से’, ‘साहित्य की चेतना’, ‘परंपरा बंधन नहीं’, ‘साहित्य का प्रयोजन’, ‘भारतीयता की पहचान’, ‘नैर्तर्य और चुनौती’, ‘व्यक्ति-व्यंजना’, ‘जीवन पर्व’, ‘नदी, नारी और संस्कृति’, ‘फागुन दुइ रे दिनी’, ‘शिरीष की याद आई’, ‘यात्राओं की यात्राएँ’, ‘बूँद मिले सागर में’, ‘जसुदा के नंदन’ और ‘गिर रहा है आज पानी’।
वे हिंदी की प्रतिष्ठा के लिए निरंतर जूझते रहे। इसके संस्कार उन्हें पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी और राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन से मिले थे। मॉरीशस से सूरीनाम तक वे विश्व हिंदी सम्मेलनों में जाते रहे। उन्होंने ‘हिंदी की शब्द संपदा’, ‘हिंदी और हमी’, ‘हिंदीमय जीवन’ और ‘प्रौढ़ों का शब्द संसार’ जैसी पुस्तकें लिखकर हिंदी की संप्रेषणीयता का दायरा बढ़ाने की कोशिश की। ‘हिंदी सेवा की संकल्पना’ जैसा ग्रंथ उन्होंने बड़े परिश्रम से संपादित किया है। हाल ही में वे स्पेन और इटली की यात्रा कर लौटे। वहाँ इंडोलॉजी के प्रख्यात विद्वान् प्रो. फिलिप्पी से उनका लंबा विमर्श भारतीय कला और दर्शन के संदर्भ में हुआ। लौटते ही कहा कि इस विमर्श को सबसे पहले हिंदी में आना चाहिए। अभी वह अनुवाद अधूरा है।
रायकृष्ण दासजी के बाद वे हिंदी के उन दो या तीन लेखकों में से थे, जिन्होंने कला और साहित्य को जोड़कर देखा और लिखा। स्व. वासुदेवशरण अग्रवाल और डॉ. रघुवीर सिंह के नाम मुझे याद आते हैं। उनका यह कार्य अद्भुत है। ‘गति और रेखा’, ‘तंत्र, कला और आस्वाद’, ‘आनंद कुमार स्वामी : परसेप्शन ऑफ वेदाज’, ‘स्वरूप विमर्श’, ‘राग-बोध और रस’ तथा ‘वैदिक सोर्सेस ऑफ इंडियन आर्ट’ उनकी वे पुस्तकें हैं, जो उनकी गहरी कलात्मक सर्जना का परिचय देती हैं। उन्होंने रामायण और गीतगोविंद जैसे ग्रंथों पर इसी दृष्टि से कार्य किया। हमारी चित्रांकन परंपरा और साहित्य के अंतर्संबंधों को उन्होंने पहली बार हिंदी में वैज्ञानिक रूप से प्रतिष्ठित करने की कोशिश की। भारतीय सौंदर्य-दृष्टि की परंपरागत व्याख्या से हटकर उन्होंने उसे लोक से जोड़ा। वे मानते थे कि कला का अर्थ है ‘खंड’, लेकिन ऐसा खंड कि जिसके बिना संपूर्ण अधूरा रहता है। उनका कहना था कि भारतीय कला की अवधारणा में केंद्र पर बल नहीं है, उसकी परिधि में आनेवाले समस्त संसार पर बल है। यह दृष्टि परंपरागत दृष्टि से भिन्न थी। यह धरातल पर टिकी हुई दृष्टि थी।
तुलसी और सूर सहित उन्होंने भारतेंदु, रहीम, रसखान, कबीर, रैदास, आलम, देव और द्विजदेव से लेकर श्यामसुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन, सत्य नारायण कविरत्न, अज्ञेय, देवेन्द्रनाथ शर्मा, गोपीनाथ कविराज, चंद्रबली त्रिपाठी और राममूर्ति त्रिपाठी तक के कृतित्व को संपादित किया। ब्रजभाषा कोश का तीन भागों में उन्होंने संपादन किया। भोजपुरी क्षेत्र के तो वे थे ही। उन्होंने ‘वाचिक कविता भोजपुरी’ नामक ग्रंथ संपादित किया। ‘अमरूक शतक’ का उन्होंने संस्कृत से हिंदी में सुंदर अनुवाद किया। इसके अलावा हिंदी की चुनिंदा कविताओं का अनुवाद उन्होंने अमेरिका में रहते ‘मॉडर्न हिंदी पोइट्री’ तथा ‘इंडियन पोइटिक ट्रेडिशन’ शीर्षक पुस्तकों में किया।
‘दस डिस्क्रेप्टिव टेकनीक ऑफ पाणिनि’ उनका सुप्रसिद्ध शोधग्रंथ है। इसके अलावा अंग्रेजी में उन्होंने ‘द इंडियन क्रिएटिव माइंड’, ‘स्टडीज इन वैदिक एंड इरानियन रिलीजन्स’ तथा ‘फॉलो द नोड्स ऑफ द फ्ल्यूट’ जैसी पुस्तकें लिखीं।
सौ से ज्यादा उनकी पुस्तकें हैं। ये धर्म, भाषा, संस्कृति, कला और लोक से लेकर हमारे व्यवहार तक पर लिखी गई हैं। वे इस देश की मनीषा के प्रतिमान व्यक्तित्व थे। ‘पद्मभूषण’ से लेकर साहित्य अकादेमी की महत्तर सदस्यता से सम्मानित उनका वैदुष्य किसी व्याख्या का मोहताज नहीं है। उनकी मनीषा इतनी प्रखर थी कि उसकी परिधि में पूरा विश्व आया। वे पूरा विश्व घूमे और हर देश में उन्होंने अपनी दृष्टि से इस देश की पहचान को स्थापित करने का ईमानदार यत्न किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद हिंदी में यही एक ऐसा व्यक्तित्व हुआ, जिसकी बहुआयामी प्रतिभा ने हमारे तमाम अनुसासनों को जोड़ने की कोशिश की। खंड से विद्रोह और समग्र के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण अपने कृतित्व के माध्यम से जताया।
हिंदी में निबंध, और विशेष रूप से ललित-निबंध, की परंपरा को उन्होंने नए धरातल पर स्थापित किया। उनकी मान्यता स्पष्ट थी। वे अडिग, आस्थावादी थे। वे कहते थे कि ‘‘वैदिक सूक्तों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविछिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है, उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। मेरी मान्यताओं का वही शाश्वत आधार है। मैं रेती में अपनी डोंगी नहीं चलाना चाहता और न जमीन के ऊपर बने रुँधे तालाबों में छपकोरी खेलना चाहता हूँ। इसलिए प्रचलित शब्दावली में अगर प्रगतिशील नहीं हूँ तो कम-से-कम प्रतिगामी भी नहीं हूँ।’’ उनके साथ रहते, उनको पढ़ते, उनसे बातें करते मैंने अनुभव किया कि उनके आचरण को कहीं उनकी अभिव्यक्ति से जोड़कर देखा गया और इसके कारण उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में नहीं समझा जा सका। वे कोरे पंक्तिपावन ब्राह्मण नहीं थे। अपने संस्कारों से वे गहरे जुड़े थे। लेकिन उनमें वैचारिक संकीर्णता नहीं थी। उनकी ग्रहणशीलता अद्भुत थी, उनका औदार्य विलक्षण था और उनकी अछोर करुणा आकाश की तरह असीम थी। वे आई.सी.एस. में जा सकते थे, लेकिन वे राहुलजी के साथ हो लिये। यायावरी करा पाठ उन्हीं से सीखा। डॉ. राममनोहर लोहिया से उनका निकट संपर्क था और रफी अहमद किदवई उनके आदर्श राजनीतिज्ञ थे। नवीनजी उनके सबसे अनन्य मित्र थे। बात-बात में नवीनजी का उद्धरण देते। ‘साहित्य अमृत’ का एक पूरा अंक ही उन्होंने नवीनजी पर निकाला। धूमिल के एक काव्य-संग्रह की उन्होंने भूमिका भी लिखा, यह जानकारी भी मुझे उनके मित्रों ने दी। स्व. श्रीपतराय उनके अभिन्न मित्र थे। यह तथ्य उनके अनुज श्री महेश्वर मिश्र ने उनके निधन के बाद मुझे बताया कि प्रेमचंद की कृतियों का सर्वप्रथम संकलन व संपादन उन्होंने पूरे मनोयोग से श्रीपतरायजी के लिए क्या और कहीं भी अपना नाम न आने का वचन श्रीपतरायजी से लिया। इस कार्य के लिए वे जो कुछ कर सकते थे, करते रहे। आशय यही है कि इन तथ्यों के आधार पर इतना जरूर जाना जा सकता है कि वे कट्टरपंथी और जड़ सर्जक नहीं थे। उनकी मान्यताएँ, उनके विश्वास और उनकी आस्था अपनी जगह स्पष्ट थी। कहीं कोई कुहासा नहीं था, भ्रम नहीं था, समझौते नहीं थे। वे अपनी जमीन पर देवदारु के वृक्ष की तरह आजीवन तने खड़े रहे।
ललित-निबंध उनकी प्रिय विद्या थी। ललित-निबंध को वे व्यक्ति-व्यंजक निबंध का छोटा सा प्रकार मानते थे। वे कहते थे कि कभी-कभी सुंदर से असुंदर अधिक छूता है। उसी तरह ललित से अधिक मनुष्य के हाथ से अनसँवरा छूता है, अनतराशा हीरा तराशे हीरे से अधिक मूल्यवान् लगता है। व्यक्ति की दृष्टि में सुंदर या ललित हो जाए—यही उनका उद्देश्य रहा। उनके लिए लिखना मरना या मरने जैसी यातना की तरह था। वे कहते थे, ‘‘अपने अनुभवों को उघारना मौत से बड़ी यंत्रणा है।’’ उन्होंने ‘स्तवक’ शीर्षक से व्यक्ति-व्यंजक निबंधों का संकलन डॉ. परमानंद श्रीवास्तव के सहयोग से निकाला, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर कुबेरनाथ राय तक के निबंध-लेखकों के प्रतिनिधि निबंध संकलित किए। हाल ही में उनके निबंधों का एक संकलन ‘व्यक्ति-व्यंजना’ के नाम से प्रकाशित हुआ है, जिसमें उनके चुने हुए 53 निबंध संकलित हैं। तब मैंने उनसे इस ग्रंथ के प्रकाशन के समय एक लंबी बात की थी। उनसे पूछा था कि आगामी सदी के भारत को वे किस रूप में देखना चाहते हैं ? उन्होंने कहा था कि मैं तो आज के अत्यंत संधिःकालीन भारत में संभावनाओं की तलाश करना चाहता हूँ। बेकार के आरोपित कालखंडों में कैद सूर्योदय की बात नहीं सोचता। उनके निबंध द्विवेदीजी की परंपरा को बहुत आगे ले जाते हैं। कुबेरनाथ राय और विवेकी राय जैसे समकालीन निबंध-लेखकों के साथ उनकी त्रयी बनती है। ठीक उसी तरह जिस तरह हरिशंकर परसाई, रवींद्रनाथ त्यागी और शरद जोशी की त्रयी व्यंग्य लेखन में है। यों निबंध विधा हमारे समकालीन लेखन में प्रायः उपेक्षित है; लेकिन यदि इस विधा की धारा नहीं सूख पाई, बल्कि और प्रवाहमय होती रही तो निस्संदेह इसका श्रेय उन्हें दिया जाना चाहिए। ‘नवभारत टाइम्स’ और ‘साहित्य अमृत’ के प्रधान संपादक के बतौर उन्होंने निबंधों को प्रमुखता से छापा। आज के जो थोड़े-बहुत निबंधकार हैं, उन्हें उन्होंने प्रश्रय दिया, उनकी हौसला-आफजाई की। अंग्रेजी के ‘पर्सनल ऐसे’ की विशेतओं से परिचित कराते हुए उन्होंने हिंदी के व्यक्ति-व्यंजक निबंधों की मौलिक परंपराओं को उद्घाटित किया और यह सिद्ध करने की कोशिश की कि हिंदी की प्रकृति के स्वतंत्र विकास का प्रमाण हिंदी में रचे गए मौलिक निबंध हैं।
उनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं—‘छितवन की छाँह’, ‘अंगद की नियति’, ‘आँगन का पंछी और बंजारा मन’, ‘कँटीले तारों के आर-पार’, ‘कौन तू फुलवा बीननिहारी’, ‘गाँव का मन’, ‘मेरे राम का मुकुट भीग रहा है’, ‘तमाल के झरोखे से’, ‘साहित्य की चेतना’, ‘परंपरा बंधन नहीं’, ‘साहित्य का प्रयोजन’, ‘भारतीयता की पहचान’, ‘नैर्तर्य और चुनौती’, ‘व्यक्ति-व्यंजना’, ‘जीवन पर्व’, ‘नदी, नारी और संस्कृति’, ‘फागुन दुइ रे दिनी’, ‘शिरीष की याद आई’, ‘यात्राओं की यात्राएँ’, ‘बूँद मिले सागर में’, ‘जसुदा के नंदन’ और ‘गिर रहा है आज पानी’।
वे हिंदी की प्रतिष्ठा के लिए निरंतर जूझते रहे। इसके संस्कार उन्हें पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी और राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन से मिले थे। मॉरीशस से सूरीनाम तक वे विश्व हिंदी सम्मेलनों में जाते रहे। उन्होंने ‘हिंदी की शब्द संपदा’, ‘हिंदी और हमी’, ‘हिंदीमय जीवन’ और ‘प्रौढ़ों का शब्द संसार’ जैसी पुस्तकें लिखकर हिंदी की संप्रेषणीयता का दायरा बढ़ाने की कोशिश की। ‘हिंदी सेवा की संकल्पना’ जैसा ग्रंथ उन्होंने बड़े परिश्रम से संपादित किया है। हाल ही में वे स्पेन और इटली की यात्रा कर लौटे। वहाँ इंडोलॉजी के प्रख्यात विद्वान् प्रो. फिलिप्पी से उनका लंबा विमर्श भारतीय कला और दर्शन के संदर्भ में हुआ। लौटते ही कहा कि इस विमर्श को सबसे पहले हिंदी में आना चाहिए। अभी वह अनुवाद अधूरा है।
रायकृष्ण दासजी के बाद वे हिंदी के उन दो या तीन लेखकों में से थे, जिन्होंने कला और साहित्य को जोड़कर देखा और लिखा। स्व. वासुदेवशरण अग्रवाल और डॉ. रघुवीर सिंह के नाम मुझे याद आते हैं। उनका यह कार्य अद्भुत है। ‘गति और रेखा’, ‘तंत्र, कला और आस्वाद’, ‘आनंद कुमार स्वामी : परसेप्शन ऑफ वेदाज’, ‘स्वरूप विमर्श’, ‘राग-बोध और रस’ तथा ‘वैदिक सोर्सेस ऑफ इंडियन आर्ट’ उनकी वे पुस्तकें हैं, जो उनकी गहरी कलात्मक सर्जना का परिचय देती हैं। उन्होंने रामायण और गीतगोविंद जैसे ग्रंथों पर इसी दृष्टि से कार्य किया। हमारी चित्रांकन परंपरा और साहित्य के अंतर्संबंधों को उन्होंने पहली बार हिंदी में वैज्ञानिक रूप से प्रतिष्ठित करने की कोशिश की। भारतीय सौंदर्य-दृष्टि की परंपरागत व्याख्या से हटकर उन्होंने उसे लोक से जोड़ा। वे मानते थे कि कला का अर्थ है ‘खंड’, लेकिन ऐसा खंड कि जिसके बिना संपूर्ण अधूरा रहता है। उनका कहना था कि भारतीय कला की अवधारणा में केंद्र पर बल नहीं है, उसकी परिधि में आनेवाले समस्त संसार पर बल है। यह दृष्टि परंपरागत दृष्टि से भिन्न थी। यह धरातल पर टिकी हुई दृष्टि थी।
तुलसी और सूर सहित उन्होंने भारतेंदु, रहीम, रसखान, कबीर, रैदास, आलम, देव और द्विजदेव से लेकर श्यामसुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन, सत्य नारायण कविरत्न, अज्ञेय, देवेन्द्रनाथ शर्मा, गोपीनाथ कविराज, चंद्रबली त्रिपाठी और राममूर्ति त्रिपाठी तक के कृतित्व को संपादित किया। ब्रजभाषा कोश का तीन भागों में उन्होंने संपादन किया। भोजपुरी क्षेत्र के तो वे थे ही। उन्होंने ‘वाचिक कविता भोजपुरी’ नामक ग्रंथ संपादित किया। ‘अमरूक शतक’ का उन्होंने संस्कृत से हिंदी में सुंदर अनुवाद किया। इसके अलावा हिंदी की चुनिंदा कविताओं का अनुवाद उन्होंने अमेरिका में रहते ‘मॉडर्न हिंदी पोइट्री’ तथा ‘इंडियन पोइटिक ट्रेडिशन’ शीर्षक पुस्तकों में किया।
‘दस डिस्क्रेप्टिव टेकनीक ऑफ पाणिनि’ उनका सुप्रसिद्ध शोधग्रंथ है। इसके अलावा अंग्रेजी में उन्होंने ‘द इंडियन क्रिएटिव माइंड’, ‘स्टडीज इन वैदिक एंड इरानियन रिलीजन्स’ तथा ‘फॉलो द नोड्स ऑफ द फ्ल्यूट’ जैसी पुस्तकें लिखीं।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book